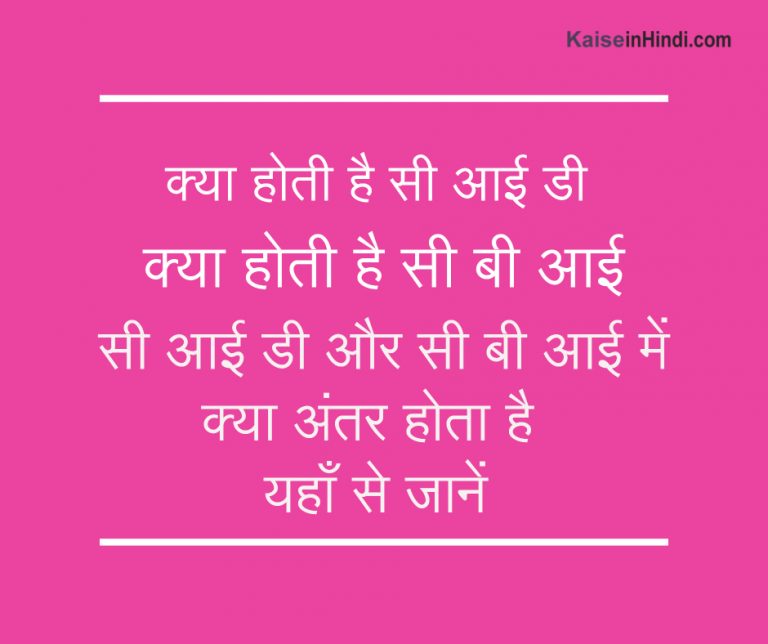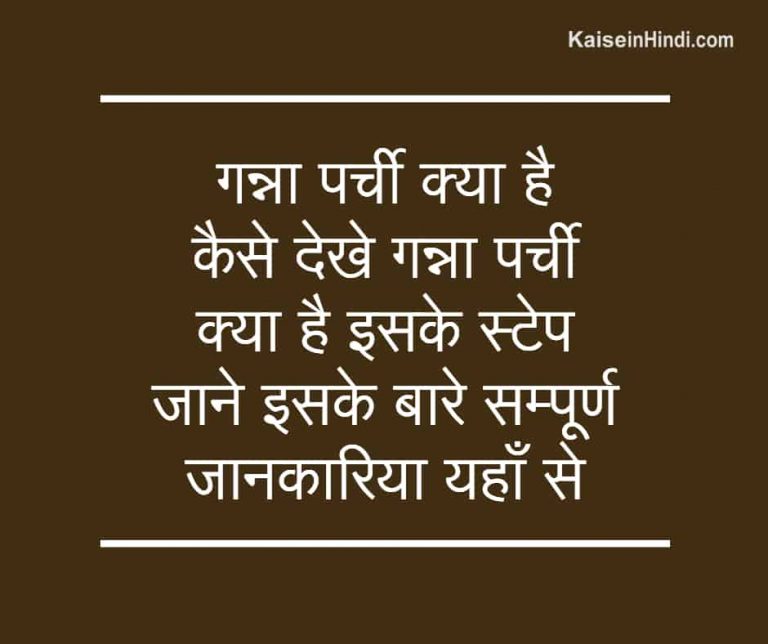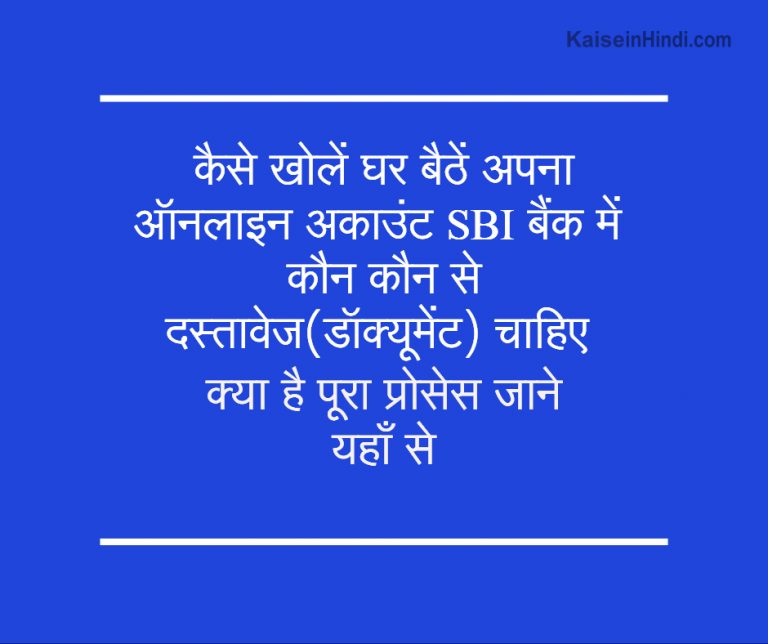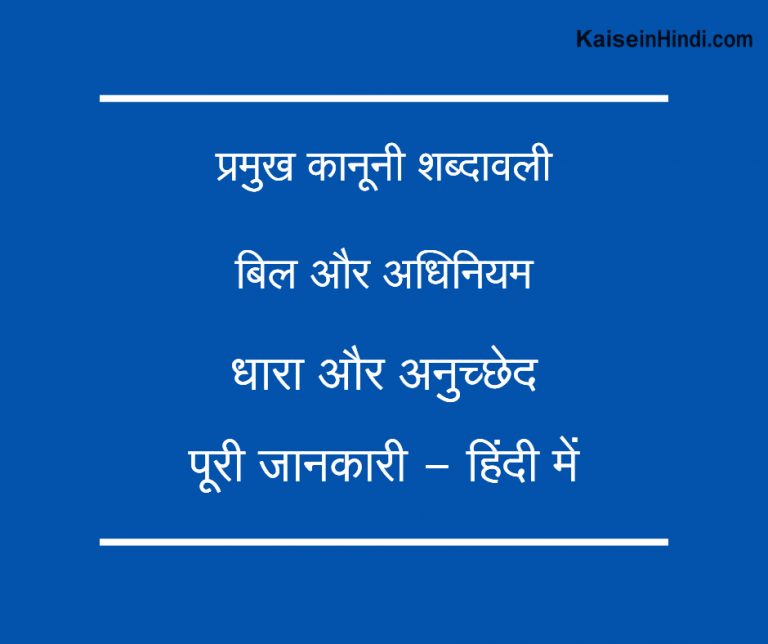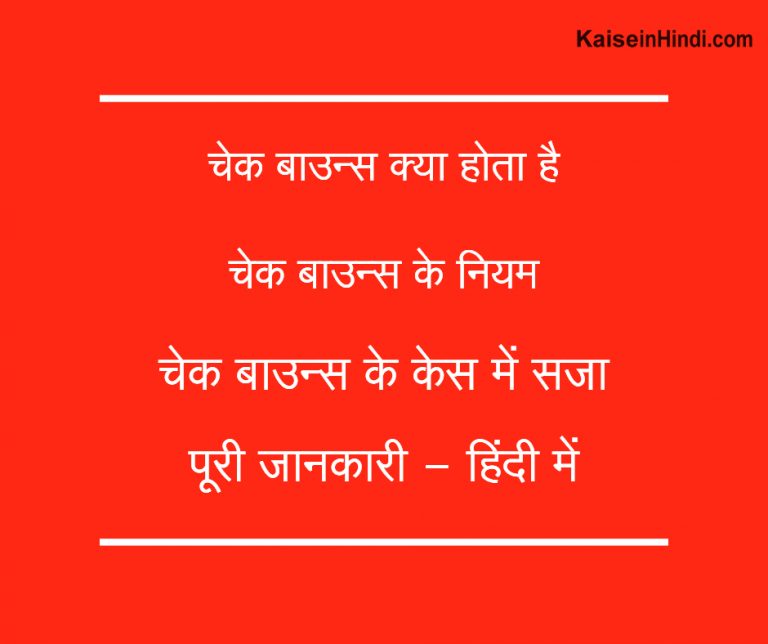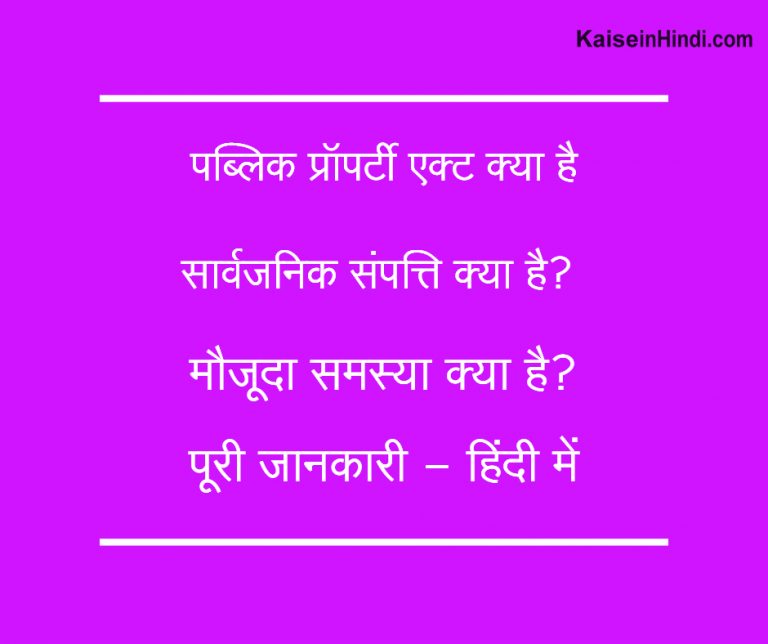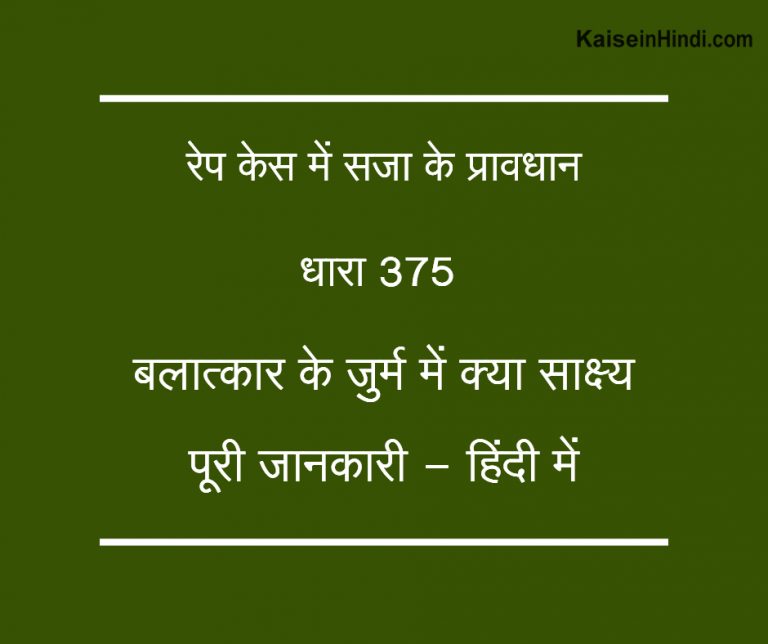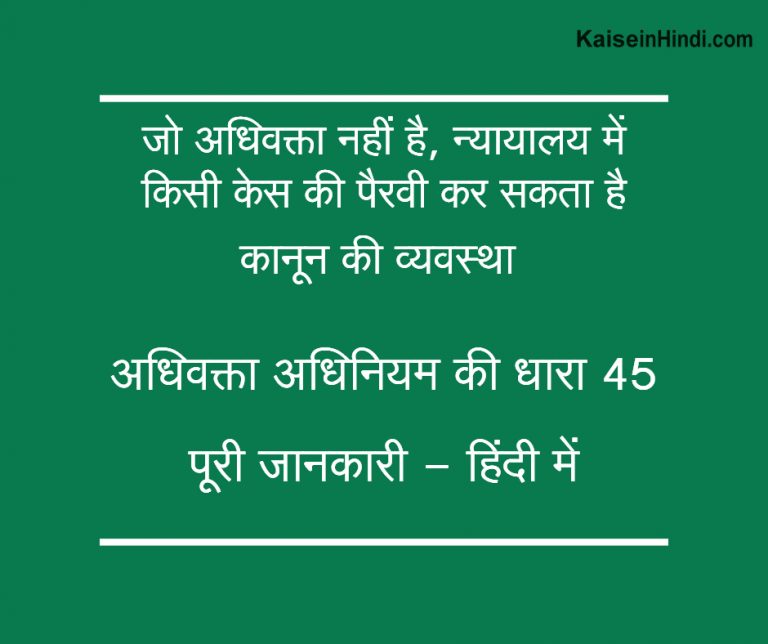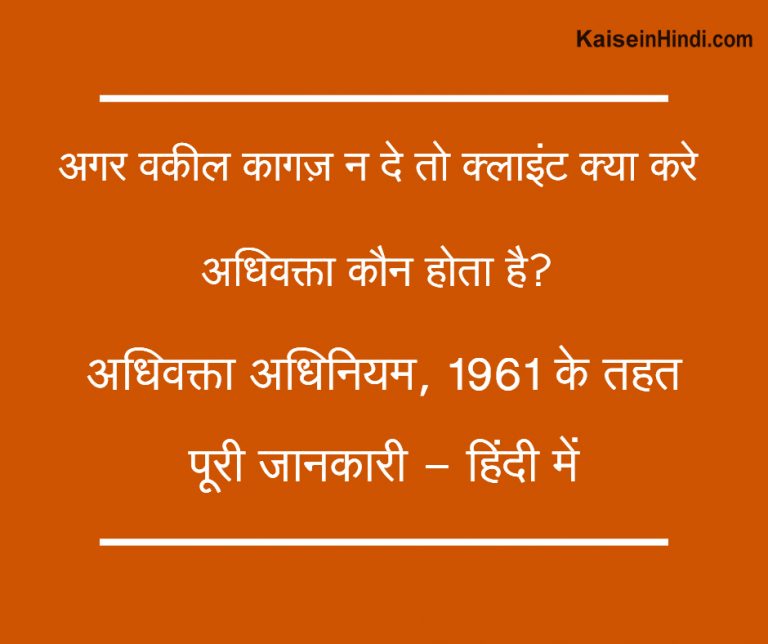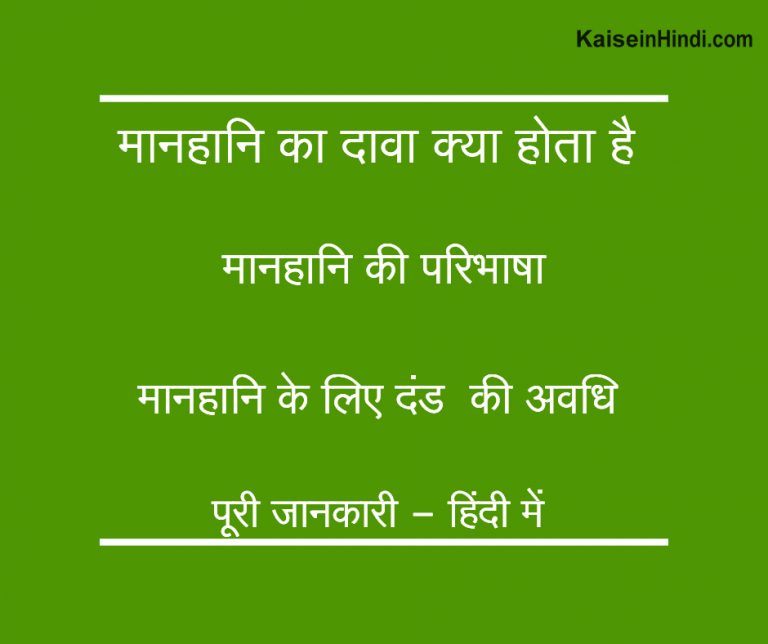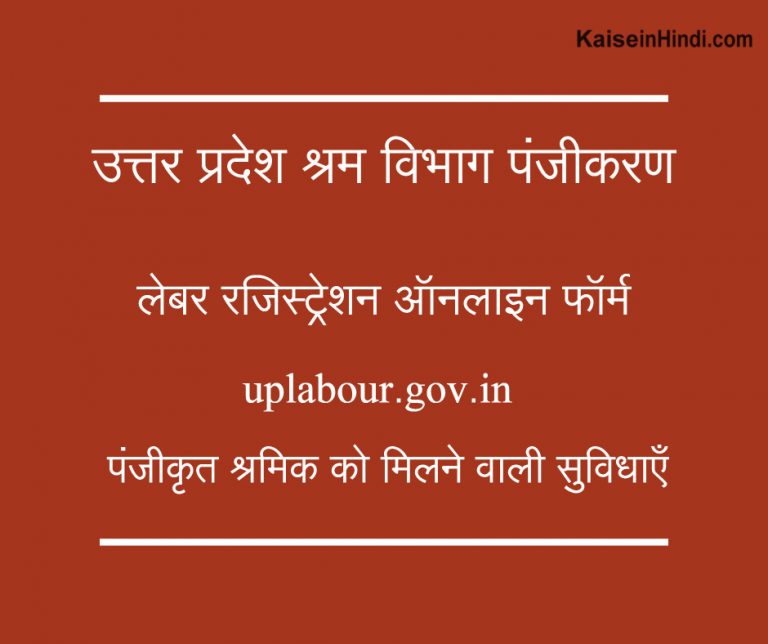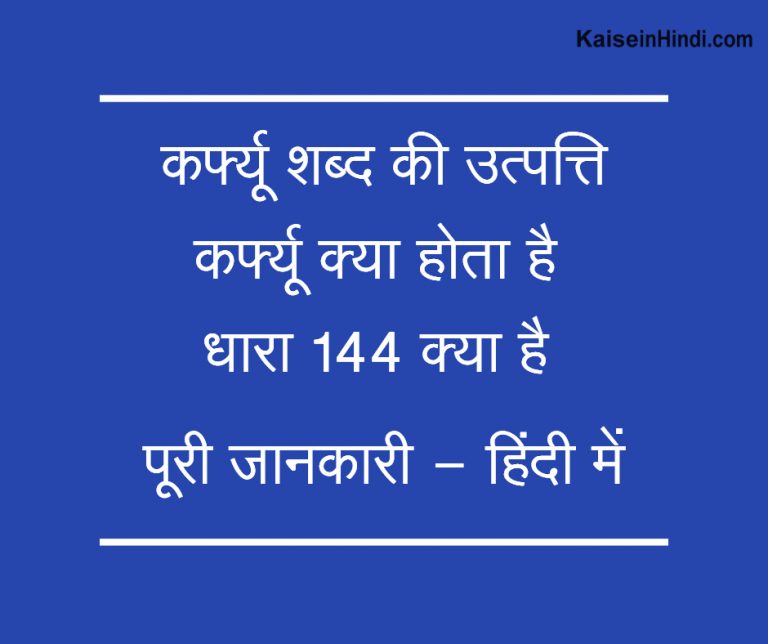किसी भी आपराधिक प्रणाली में शासन द्वारा दंड का प्रावधान बनाया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध न करें और भयभीत रहे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और अपराध समाज में न हो । भारत के दंड संविधान में भी दंड का वर्णन किया गया है, भारतीय दंड संविधान की धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं तथा इसी दंड के प्रकारों में आजीवन कारावास के विषय में बताया गया है । इस लेख के द्वार भारत में चलनसार दंड एवं आजीवन कारावास को बताया जा रहा है । किसी समय समाज में बहुत तरह के दंड चलनसार थे, लेकिन समय और सभ्यताओं के साथ दंड को बहुत कम कर दिया गया है । आजीवन कारावास यानि उम्रकैद की सज़ा गंभीर अपराधों के लिए बनाई गयी है । भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 में अपराधों के दंड के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है ।
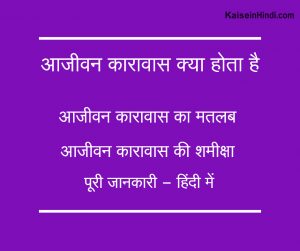
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत दंड के प्रकार
- मृत्यु
- आजीवन कारावास
- कारावास
- संपत्ति का संपहरण
- जुर्माना
मृत्यु दंड
मृत्युदंड एक अलग तरह का दंड है जिसे भारतीय दंड संविधान की धारा 53 में बताया गया है । इस दंड में व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा मृत्यु देने का प्रवाधान है । किसी भी समय इस तरह की मृत्यु अलग – अलग प्रकार से दी जाती थी परंतु अब अपराधियों को केवल फांसी के द्वारा देने का प्रवाधान है तथा यह फांसी भी जनता के समक्ष्य नहीं होती है, बल्कि गोपनीय रूप से दी जाती है । सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने पर भारत में प्रतिबंध लगाई गई है तथा केवल राज्य सरकार द्वारा गोपनीय रूप से मृत्युदंड के अपराधी को फांसी दी जाएगी ।
संविधान किसे कहते है, लिखित संविधान का क्या अर्थ है ?
आजीवन कारावास
आजीवन कारावास को इस लेख में विस्तार रूप से आगे समझया जाएगा ।
निर्वासन
निर्वासन दंड के रूप में पहले दिया जाता था लेकिन इस प्रकार के दंड को अब हटा दिया गया है ।
कारावास
भारतीय दंड संहिता में अपराधों के संदर्भ में दिया जाने वाला करावास दो प्रकार का कारावास हो सकता है ।
(1) कठिन और कठोर कारावास के अलावां मेहनत ।
(2) साधारण कारावास।
संपत्ति का संपहरण
(1) अगर, धारा 105घ के तहत जांच, खोज या सर्वेक्षण के फलस्वरूप न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या कोई संपत्ति, जुर्म का उत्पत्ति है तो वह ऐसे व्यक्ति पर (जिसे इसमें इसके बाद प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह उस सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के अंदर उस आय, उपार्जन या आस्तियों के वे स्त्रोत, जिनसे या जिनके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति जुटाई है, वह साक्ष्य जिस पर वह आशा करता है तथा अन्य युक्त जानकारी और विशिष्टियाँ उपदर्शित करे और यह कारण बताए कि, यथास्थिति ऐसी सभी या किसी संपत्ति को अपराध का उत्पत्ति क्यों न घोषित किया जाए और उसे केन्द्रीय सरकार को क्यों न समपहृत कर दिया जाए ।
(2) जहाँ किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के तहत सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है वहाँ सूचना की एक प्रति की ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी तामील की जाएगी ।
जुर्माना
जुर्माना तमाम प्रकार के अपराधों में देना पड़ता है । परन्तु जुर्माना अपराध को देखते हुए लगाया जाता है कि जिस प्रकार से अपराध होता है उसके हिसाब से जुर्माना भरना पड़ता है |
आजीवन कारावास
हमारे यहाँ आजीवन कारावास के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं तथा आजीवन कारावास के बारे में बहुत सारी बातें कहने और सुनने को मिलती हैं । इसके विषय में बात साफ होनी चाहिए । आजीवन कारावास का क्या मतलब है? कुछ व्यकित आजीवन कारावास को 20 वर्ष ही बताते हैं । कुछ व्यकित आजीवन कारावास को 14 वर्ष ही बताते हैं । कुछ व्यकित रात और दिन को अलग-अलग कारावास बताते हैं । जब भी कोई न्यालय किसी अपराध के लिए किसी व्यकित को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है तो प्रणाली के समक्ष इस कारावास की अवधि का मतलब सज़ा पाने वाले व्यक्ति की बची हुई जिंदिगी का होता है । अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन जेल में व्यतीत करेगा । यही आजीवन कारावास का मतलब है जिसकी व्याख्या उच्चा न्यालय ने भी अपने फैसलों में सुनाया है ।
आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष का सजा नहीं होता
हमारे समाज में आजीवन कारावास को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रान्तियाँ हैं, जो कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास बताते है |, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हैं । यह शेष बचे जीवन का कारावास होता है ।
मोहम्मद मुन्ना बना यूनियन ऑफ इंडिया (एआईआर 2005 एस सी 3440) केघटना में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि आजीवन कारावास का मायने कठोर आजीवन (जीवनपर्यंत) कारावास से है । यह 14 या 20 वर्ष के सजा के अनुरूप नहीं है । आजीवन कारावास से दंडित अपराधी को बंदीगृह में रखा जाने का प्रावधान किया जा सकता है । एक घटना खोका उर्फ प्रशांत सेन बनाम बीके श्रीवास्तव का भी है । इस घटना में उच्चतम न्यालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आजीवन कारावास का मायने 20 वर्ष की अवधि के कारावास से ना होकर अपराधी का संपूर्ण जीवनपर्यंत कारावास से है ।
आजीवन कारावास के दंड का संक्षिप्त करना
भारतीय दंड संहिता आजीवन कारावास के दंड को संक्षिप्त करना के संदर्भ में समझती है । भारतीय दंड अधिनियम की धारा 55 में आजीवन कारावास को संक्षिप्त करना का नियम बनाया गया है । इस नियम के तहत भ्रांतियां का उत्पत्ति होता है ।
कोई भी उपयुक्त सरकार किसी भी घटना में आजीवन कारावास का दंड आदेश दिया गया हो किसी अपराधी की अनुमति के बिना भी आजीवन कारावास को कम की जा सकती है । अगर आजीवन कारावास को कम किया जाता है तो आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तक की होगी अन्यथा किसी भी आजीवन कारावास को यदि उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया जा रहा है तो वह कारावास 14 वर्ष से भी काम हो सकता है । अपराधी को चौदह साल के पूर्व ही छोड़ दिया जाएगा ।
भारतीय दंड अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य को दी गई यह दो बड़ी अधिकार है, जिसमें वह अपने अधिकार के माध्यम से किसी भी आजीवन कारावास से दंडित अपराधी के कारावास को कम कर सकती है । 14 साल से कम की कितनी भी समय के लिए व्यक्ति को कारावास दी जा सकती है ।
परंतु भारत दंड अधिनियम की धारा 433 (ए) के तहत एक लांछन भी दिया गया है । जिस लांछन के फल स्वरूप यदि व्यक्ति को ऐसे अपराध के घटना में आजीवन कारावास दिया गया है, जिस जुर्म में मृत्युदंड यानि जान से मार दिए जाने का नियम था परंतु मृत्युदंड यानि जान से मार देने के अलावां अपराधी को आजीवन कारावास दिया गया है तो ऐसी समस्यों में उपयुक्त सरकार आजीवन कारावास को कम करती है तो कम करने की समय कम से कम 14 साल की होगी । 14 साल से कम समय को नहीं किया जा सकता है ।
यह भी पढ़ें: गिरफ्तारी के बाद जमानत कैसे प्राप्त करें?
डेथ वारंट (Execution Warrant) क्या होता है
इस नियम के अनुसार समाज में ऐसी भ्रांतिया फैलती है कि आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है लेकिन यह कारावास आजीवन कारावास नहीं माना जाता है यह तो उपयुक्त सरकार द्वारा कम किया गया कारावास होता है ।
सिद्धार्थ वशिष्ठ @ मनु शर्मा बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में जेसिका लाल नामक महिला की हत्या के अपराधी मनु शर्मा ने अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर पेश की थी कि वह चौदह साल का कारावास बिताने के पश्चात आजीवन कारावास से मुक्त होने का अधिकार रखता है ।
उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कहा कि मुक्त करने का आदेश उपयुक्त सरकार द्वारा दी जा सकती है और इसके विषय में उच्चतम न्यायालय कोई दिशानिर्देश नहीं जारी कर सकता ।
इस घटना में पहले दंड समीक्षा बोर्ड द्वारा अपराधी को चौदह साल के कारावास के पूरे हो जाने के पश्चात छोड़ दिए जाने से उपयुक्त सरकार ने मना कर दिया था ।
उच्चतम न्यायालय ने इसे उपयुक्त सरकार का अधिकार माना है । अपराधी को मुक्त करना न करना अपराधी के चरित्र पर निर्भर करता है । यह चरित्र कैसा होगा इसे तय करने का कार्य सरकार द्वारा बनाई गयी दंड समीक्षा बोर्ड को होगा ।
आजीवन कारावास की समीक्षा
भारत दंड अधिनियम की धारा 57 के तहत आजीवन कारावास की समीक्षा के संदर्भ में समझाया गया है । यदि किसी समस्या में आजीवन कारावास की शमीक्षा करनी पड़ती है तो ऐसी समीक्षा करने के लिए भारतीय दंड अधिनियम की इस धारा को उपयोग में लाया जाता है । इस धारा के तहत आजीवन कारावास को 20 साल का कारावास माना गया है, 20 साल के कारावास के अनुरूप माना गया है ।
समय-समय पर दंड की ऐसी समीक्षा की आवश्यकता पड़ती रहती है । इस आवश्यकता की भरपाई के लिए भारतीय दंड अधिनियम की धारा 57 में आजीवन कारावास की समीक्षा के लिए एक समय निर्धारित की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया जाता है तो उसे 20 वर्ष की समय बिता लेने के पश्चात मुक्त कर दिया जाएगा । आजीवन कारावास का मतलब शेष बचे जीवन का कारावास होता है ।
भारतीय संविधान में कितनी भाषा है
दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजीवन कारावास का संक्षिप्त करना
भारत की दंड प्रक्रिया अधिनियम के तहत भी आजीवन कारावास के संक्षिप्त करना के संबंध में समझाया गया है । धारा 433 के तहत उपयुक्त सरकार को आजीवन कारावास को कम किए जाने की अधिकार दी गई है । यह धारा 433 (ए) के तहत ऐसी अधिकार पर निर्बंधन भी लगाए गए हैं ।
धारा 433 के तहत उपयुक्त सरकार किसी आजीवन कारावास के अपराधी का कारावास कम करती है । अगर अपराधी को किसी ऐसे जुर्म में आजीवन कारावास दिया गया है जिस अपराध में मृत्युदंड भी दिया जा सकता था तो ऐसे कारावास को यदि उपयुक्त सरकार कम करती है तो केवल 14 वर्षों से के पश्चात के समय का कारवास कम कर सकती है या खत्म कर सकती है, अन्यथा अपराधी को कम से कम 14 वर्ष का कारावास तो व्यतीत करना ही होगा ।
एस निंगप्पा गन्दावर बनाम कर्नाटक राज्य के घटना में भी उच्चतम न्यायालय अपराधी द्वारा बालक की हत्या को घोर जुर्म मानते हुए आदेश दिया कि सरकार अभियुक्त के आजीवन कारावास को 14 साल की समय से कम ना करे ।
अशोक कुमार बनाम भारत संघ के विवाद में भी दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा 433 से एवं दंड अधिनियम संशोधन अधिनियम 1982 से जुड़ा है । इस घटना में उच्चतम न्यायालय ने साफ – साफ दिशानिर्देश दिए हैं तथा अंत में अपने निर्णय में यह भी कहा है कि किसी भी समस्या में सरकार द्वारा किसी अपराधी को 14 साल के कारावास को व्यतीत करने के पश्चात ही मुक्त किया जाएगा ।
अगर वह अपराधी किसी ऐसे जुर्म से लिप्त पाया गया है जिस जुर्म में आजीवन कारावास के अतिरिक्त मृत्युदंड देने का विधान भी रखा गया है । रात और दिन के लिए अलग – अलग दिन की समीक्षा नहीं की जाती है बल्कि 24 घंटे का 1 दिन माना जाता है ।
इस लेख में हमने आप को आजीवन कारावास का मतलब और दंड के प्रकार इसके विषय में विस्तार से जानकारी दी है अगर आप के मन में इस लेख से संबंधित कोई प्रश्न हैं तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं हम आप के द्वारा की प्रतक्रिया का आदर करेगें |